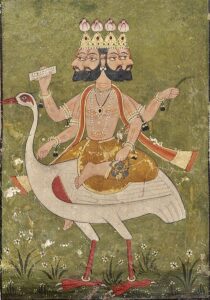खाद्यान्न का अपव्यय दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। सभी देश भोजन की बर्बादी रोकने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पूर्ण रूप से इसमें सफलता मिलना मुश्किल है, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? यह बड़ा सवाल है। सर्वप्रथम तो हमें खाद्यान्न को बर्बाद होने से रोकने के उपाय करने चाहिए, और फूड वेस्ट से पैसा कैसे कमाया जाए ये भी सीखना चाहिए।
फूड वेस्ट के विषय में यहां पर हम बात करें तो, एक तरफ हम महंगाई से त्रस्त हैं। महंगाई के कारण जीना मुश्किल होता जा रहा है। जब की दूसरी और हम अनाज, फलों और सब्जियों को बर्बाद करने से पीछे नहीं हटते। घर-होटल-रेस्तरां या भोज में भोजन उतना ही बेकार करते है जितना की भोजन।
भारत अमरीका सहित दुनिया में 40% अन्न बर्बाद हो जाता है
चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। क्या आप जानते है भारत में उत्पादित भोजन का लगभग 40% अन्न बर्बाद हो जाता है? पर्याप्त खाद्य उत्पादन के बावजूद, UN के मुताबिक लगभग 19 करोड़ भारतीय कुपोषित हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में खाद्य अपव्यय का मूल्य लगभग 92,000 करोड़ प्रतिवर्ष है।
फूड सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2017 के अनुसार, प्रति व्यक्ति सबसे कम खाद्य अपशिष्ट उत्पादन वाले देशों में ग्रीस और चीन (प्रति वर्ष 44 किग्रा) शामिल हैं। इसके बाद भारत (51 किग्रा) है। सर्वाधिक अपशिष्ट निर्माण वाले देश ऑस्ट्रेलिया (361 किलोग्राम) हैं, इसके बाद अमेरिका (278 किलो) हैं।
Related video : https://www.youtube.com/watch?v=660RdeA9xCQ
भारत में आवश्यकता से भोजन का अधिक उत्पादन
भारत को हर साल 235-240 मिलियन टन भोजन की आवश्यकता होती है। जिसके सामने 2018-19 में 283.37 मिलियन टन भोजन का उत्पादन किया गया था। इसका मतलब है कि देश में भोजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन 40% भोजन बर्बाद हो जाना एक बड़ी समस्या है।
अब प्रश्न ये उठता है की खाद्य अपव्यय को रोकने के लिए हमे क्या करना चाहिए? सर्व प्रथम तो इसके लिए हमे स्वयं जागरूक बनकर, हमारे घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। दूसरा होटल-रेस्तरां, शादी-ब्याह और पार्टियों में खाने के अपव्यय को रोकना होगा। तीसरा, स्वयं और सरकार को भोजन की बर्बादी रोकने का अभियान शुरू करना पड़ेगा।
बाबा रामदेव और उनके जैसे अन्य व्यक्ति तथा कंपनीया देश में कोल्ड स्टोरेज की श्रृंखला स्थापित करे

यहां हम विभिन्न देशों के विद्वानों के कुछ दिलचस्प निष्कर्ष देखेंगे। संभव है कि ये चौंकाने वाले निष्कर्ष और इसके पीछे के कारणों को जानने से, हमें इस समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। और इस समस्या का समाधान खोज कर फूड वेस्ट से पैसा कैसे कमाया जाए इसकी अनेक तरकीब भी मिलेगी।
वर्तमान में, दुनिया के खाद्य कचरे में 47 लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होता है। विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार, दुनिया के अधिकांश देशों में लगभग 40 प्रतिशत भोजन बर्बाद हो जाता है।
एक अध्ययन के अनुसार, दुनिया में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, भारत हर साल कुल उत्पादन का 18% सब्जियों को बर्बाद करता है। इसके पीछे मुख्य कारण कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटर ट्रांसपोर्ट की कमी माना जाता है। खाद्यान्न, फल और सब्जियों के नुकसान से हर साल करोड़ों रुपये का नुकसान होता है।
देश में केवल 7,645 कोल्ड स्टोरेज दोगुना से ज्यादा की जरूरत
वर्तमान में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, देश में केवल 7,645 कोल्ड स्टोरेज हैं। इसकी क्षमता 37-39 मिलियन टन (MT) है। जो कि दोगुना होकर लगभग 75 मिलियन मीट्रिक टन होना चाहिए। इसके लिए 65,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश की आवश्यकता है।
यदि बाबा रामदेव और उनके जैसे अन्य व्यक्ति तथा कंपनीया आगे आकर देश के हर कोने में कृषि उपज के उचित रखरखाव के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करते है, तो स्वार्थ के साथ परमार्थ किया जा सकता है।
भारत में कुल राज्यों में से केवल चार राज्यों में विनिर्माण क्षेत्र के पास कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है। अन्य 24 राज्यों में ऐसी सुविधा नहीं है।
भारत में करोड़ों रुपये का सरकारी खाद्यान्न बर्बाद
ओम प्रकाश शर्मा नाम के एक आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा 2013 में दायर एक आरटीआई के जवाब में, भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने स्वीकार किया कि 2005 से 2013 के बीच, भारत में करोड़ों रुपये के 1,94,502 मीट्रिक टन सरकारी खाद्यान्न बर्बाद हो गया।
अगर हम अमेरिका में इस समस्या के बारे में बात करते हैं, तो अमेरिका में उत्पादित सभी प्रकार के भोजन में से 40% भोजन बर्बाद या खराब हो जाता है। दूसरी ओर, 50 मिलियन अमेरिकी भोजन प्राप्त करने के बारे में असुरक्षित हैं। कई मामलों में, भोजन की बर्बादी के कारण लोगों और प्रणाली पर कीमतों का बोझ पड़ता है।
अमेरिकी हर साल 5 165 बिलियन मूल्य के भोजन को फेंक देते हैं। संयुक्त राज्य में, प्रत्येक वर्ष चार परिवार 1,600 मूल्य के भोजन को बर्बाद कर देते हैं। अमेरिका में हर छह में से एक अमेरिकी भूखा मर रहा है।
सिंगापुर भोजन की बर्बादी के बारे में बहुत सचेत
सिंगापुर में हुए एक हालिया सर्वेक्षण में पता चला है कि वहां पर 10 में से 9 लोग भोजन की बर्बादी के बारे में बहुत सचेत हैं। वहां के ज्यादातर लोगों का मानना है कि खाद्य और पेय कंपनियों को अपने अनसोल्ड और निकट-समाप्ति की तारीख वाले उत्पादों को सस्ते दाम पर वितरित करना या बेचना चाहिए , जो कि जरूरतमंदों के लिए खाद्य हैं।
फिर भी राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसी के अनुसार, सिंगापुर में पिछले 10 वर्षों में खाद्य अपशिष्ट की मात्रा में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
यह संख्या सिंगापुर की बढ़ती आबादी और आर्थिक गतिविधि के साथ बढ़ने की उम्मीद है।
सर्वेक्षण में पाया गया कि सिंगापुर के प्रमुख होटलों, रेस्तरां और आउटलेट्स में से फेयर प्राइस FairPrice, ब्रेडटॉक BreadTalk, मैकडॉनल्ड्स McDonald’s और कोल्ड स्टोरेज Cold Storage अपने भोजन की बर्बादी को कम करने में सक्षम हैं।
सिंगापुर के प्रमुख होटलों, रेस्तरां और आउटलेट्स में अनसोल्ड और निकट-समाप्ति की तारीख वाले उत्पादों के सस्ते दाम तथा फ्री
सिंगापुर की यह कंपनियां भोजन की बर्बादी कम करती हैं। इसे पूरा समर्थन दिया जाता है। इस ऑपरेशन में, 10 में से 8 कंपनियां उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता फैलाकर खाद्य अपशिष्ट की मात्रा को कम करने में सक्षम हुई हैं। और 10 में से 7 कंपनियां लगातार अपने आउटलेट पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
FairPrice आउटलेट्स पर किसी भी कारण से खाने की चीजे और सब्जियां अप्रयुक्त (Unused ) रहती हैं, तब इसे सुपरमार्केट श्रृंखला द्वारा छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, और नई पैकेजिंग में कम कीमतों पर बेचा जाता है। बाद में इसका उपयोग खाद्य कचरे को खाद बनाने के लिए किया जाता है।
सुपरमार्केट श्रृंखला के सेंगक्सियॉन्ग ShengSiong के प्रवक्ता के अनुसार, कंपनी ने food waste रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। समाप्ति तिथि के पास खाद्य पदार्थों में कर्मचारियों को छूट प्रदान करते हैं, और ड्राइवरों को वस्तुएं देते हैं ताकि वे अपने परिवार और दोस्तों को भोजन की बर्बादी से निपटने के लिए वितरित कर सकें।
प्रमुख होटलों, रेस्तरां, आउटलेट्स और सुपरमार्केट श्रृंखला द्वारा इस प्रकार की चीजे दान भी की जाती है।
फूड रीसाइक्लिंग मशीन बनाकर फूड वेस्ट से पैसा कैसे कमाया जाए

अब बात करते है फूड वेस्ट से पैसा कैसे कमाया जाए। आजकल अधिकतर घरों में आटा चक्की, फ्रिज, वाशिंग मशीन इत्यादि होना आम बात हो गई है। अब तो डिशवॉशर मशीन और खाद्य तेल बनाने का मशीन भी लोग खरीद रहे हैं। ऐसे में हमे घर में इस्तेमाल हो सके वैसा अच्छा फूड रीसाइक्लिंग मशीन बनाना चाहिए।
आप शायद जानते है, एक चीज जो आम तौर पर खाद्य अपशिष्ट से निकलती है वह है खाद। आजकल किचन गार्डेन और होम गार्डेन मे ऑर्गेनिक खाद का अधिक इस्तेमाल होता है। जो की आप घरेलु फूड वेस्ट से उत्पन्न कर सकते है।
सब्जी मंडी, होटल, रेस्तरां, शादी-ब्याह, बर्थडे और कई सारी पार्टियों में जो फूड वेस्ट निकलता है, उसके रीसाइक्लिंग से खाद बनाने के लिए, बड़े खाद्य अपशिष्ट रीसाइक्लिंग मशीनों का निर्माण और बिक्री भी किया जा सकता है।
मोबाइल ऐप और वेबसाइट बनाकर फूड वेस्ट से पैसा कैसे कमाया जाए

फूड वेस्ट एकत्रित करना और उसका रीसाइक्लिंग करना भी एक व्यवसाय है। छोटी बड़ी पार्टियों में होने वाली दावत और भोज से एवं होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल वगैरह जगहों पर, बचा हुआ खाना तथा फूड वेस्ट एकत्रित करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाना चाहिए।
फूड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मोबाइल ऐप और वेबसाइट बनाकर, खाना इकट्ठा करने और वितरित करने के लिए स्वयंसेवकों का नेटवर्क भी खड़ा करना चाहिए। इससे अच्छा खाना जरूरतमंद लोगों में बांटने का, और फूड वेस्ट के जरिए पैसा कमाने का काम किया जा सकता है।
जैविक उर्वरक कंपनी शुरू करके फूड वेस्ट से पैसा कैसे कमाया जाए

Related Content : https://startayurvedic.in/how-long-will-we-consume-poisonous-food/
रासायनिक उर्वरकों Fertilizer के व्यापक उपयोग से खान पान जहरीला और धरती बंजर बन रही है। इसलिए अब खेतों, बागानों में जैविक उर्वरक का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आप इसका फायदा उठाकर ऐसी कंपनी शुरू कर सकते हैं, जो खाद्य कचरे को वाणिज्यिक उर्वरक में बदल देती है। इस प्रकार आप एक जैविक उर्वरक कंपनी शुरू कर सकते है।
दुनिया में लाखों लोग भूखे सोते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है, और हम अन्नदेव का अनादर करते हुए खाना बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपना सुधार ही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। हमें खाना बर्बाद नहीं करने की शुरुआत हमारे घर से ही करनी चाहिए, और जाहिर समारंभ में कम से कम खाना बर्बाद हो इसके लिए जागरूकता फैलानी चाहिए।















 स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। सूर्य नमस्कार, एरोबिक, योग तथा अन्य व्यायाम से शरीर में शक्ति तथा रोगप्रतिकारक क्षमता में वृद्धि होती है।
स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। सूर्य नमस्कार, एरोबिक, योग तथा अन्य व्यायाम से शरीर में शक्ति तथा रोगप्रतिकारक क्षमता में वृद्धि होती है।

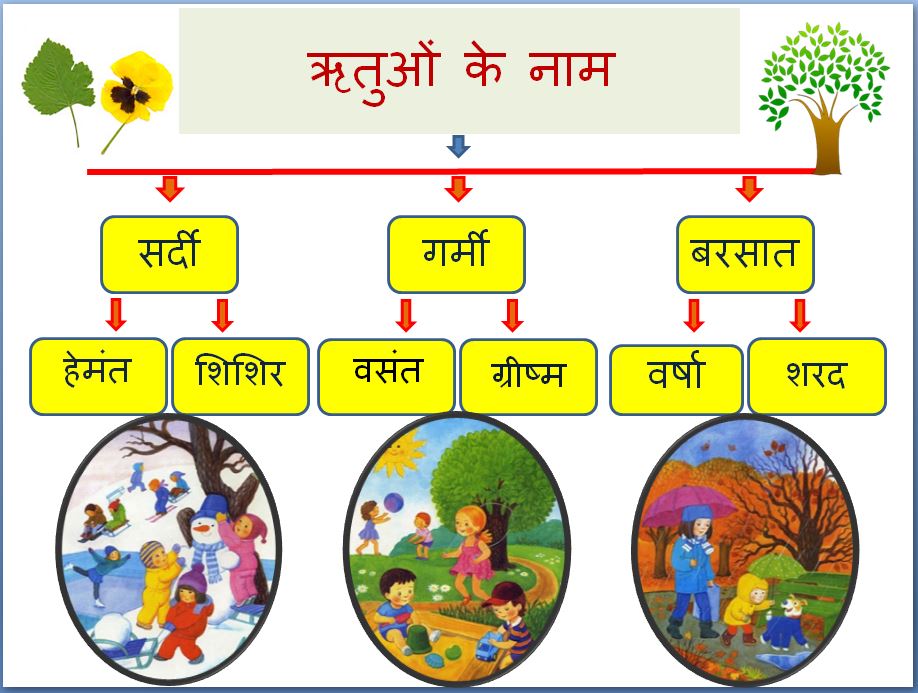
















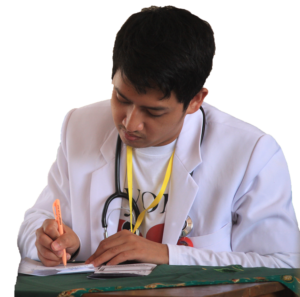 जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तब तुरंत उसे डॉक्टर याद आता है। ज्यादातर लोग अपने घर के आसपास एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाकर दवाई ले लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। पर क्या छोटी मोटी हर एक बीमारी में डॉक्टर के पास दौड़ना सही है? हो सकता है आपकी बीमारी का इलाज आसान हो और घर पर ही हो सकता हो। आजकल के पढ़े-लिखे लोगों को एलोपैथी ट्रीटमेंट की कमियां और एलोपैथिक दवाइयों की साइड इफेक्ट के बारे में पता चलने लगा है। अब देश-विदेश में भी आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पर लोगों का भरोसा बढ़ने लगा है। तब बहुत से लोगों के मन में एक सवाल होता है कि होम्योपैथी और आयुर्वेद में क्या अंतर है?
जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तब तुरंत उसे डॉक्टर याद आता है। ज्यादातर लोग अपने घर के आसपास एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाकर दवाई ले लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। पर क्या छोटी मोटी हर एक बीमारी में डॉक्टर के पास दौड़ना सही है? हो सकता है आपकी बीमारी का इलाज आसान हो और घर पर ही हो सकता हो। आजकल के पढ़े-लिखे लोगों को एलोपैथी ट्रीटमेंट की कमियां और एलोपैथिक दवाइयों की साइड इफेक्ट के बारे में पता चलने लगा है। अब देश-विदेश में भी आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पर लोगों का भरोसा बढ़ने लगा है। तब बहुत से लोगों के मन में एक सवाल होता है कि होम्योपैथी और आयुर्वेद में क्या अंतर है?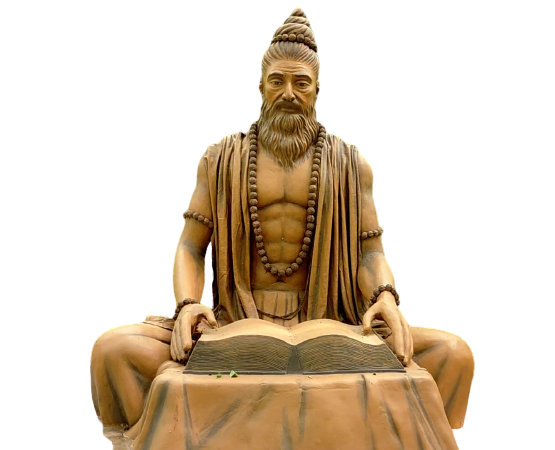
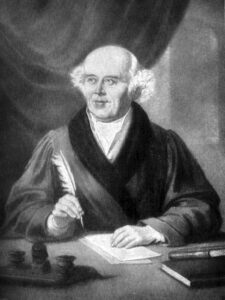 होम्योपैथी के जन्मदाता सैम्यूल क्रिश्चियन हानेमान का जीवन
होम्योपैथी के जन्मदाता सैम्यूल क्रिश्चियन हानेमान का जीवन








 हुआ यूं कि हमारे साथ आए हुए स्थानीय कार्यकर्ता ने भी हमारी तरह सावन का व्रत रखा हुआ था फिर भी भूख लगने पर वो हमारे साथ आलू की वेफर्स और आलू का फराली चिवडा नहीं खा रहा था। जब भी हम उसे वेफर्स देते थे तब वो खाने से मना कर देता था। ऐसा दो तीन बार हुआ इसलिए मैंने उसे पूछा कि वेफर्स क्यों नहीं लेता? तब उस कार्यकर्ता ने कहा कि ‘इन सभी फराली चीजों मे आलू होता है और में आलू नहीं खाता’।
हुआ यूं कि हमारे साथ आए हुए स्थानीय कार्यकर्ता ने भी हमारी तरह सावन का व्रत रखा हुआ था फिर भी भूख लगने पर वो हमारे साथ आलू की वेफर्स और आलू का फराली चिवडा नहीं खा रहा था। जब भी हम उसे वेफर्स देते थे तब वो खाने से मना कर देता था। ऐसा दो तीन बार हुआ इसलिए मैंने उसे पूछा कि वेफर्स क्यों नहीं लेता? तब उस कार्यकर्ता ने कहा कि ‘इन सभी फराली चीजों मे आलू होता है और में आलू नहीं खाता’।